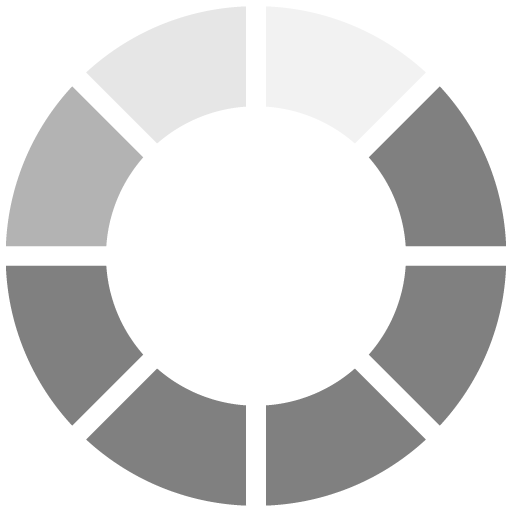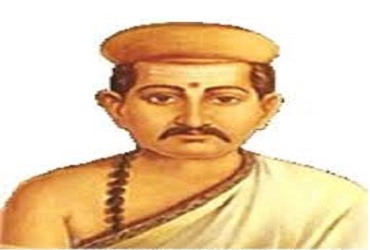
विद्यापति और मिथिला की चित्रकला के बीच एक गहरा संबंध दिखाई पड़ता है। विद्यापति के गीत और चित्रकला मिथिलांचल के जीवन के कण-कण में समाहित हैं।मिथिला की लोक चित्रकला विद्यापति का जन्म 1360 ई. के आसपास अनुमानित है। इससे काफी पूर्व से प्रचलन में रही है। इसे बहुत दिनों तक मधुबनी चित्रकला कहा गया।
प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे-धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों,दीवारों एवं कागज पर उतर आयी है। माना जाता है कि ये चित्र राजा जनक ने राम-सीता के विवाह दौरान महिला कलाकारों से बनवाये थे। पहले महिलाएँ इस कला में थीं,अब पुरुष भी सक्रिय हो गये हैं। अपने असली रूप में ये पेंटिंग गाँव की मिट्टी से लीपी गई झोपड़ियों में दिखती है,लेकिन इसे कपड़े या पेपर या कैनवास पर भी बनाया जाता है। देवी-देवताओं की तस्वीर,प्राकृतिक नजारे एवं विवाह के दृश्य इस पेंटिंग की विषय-वस्तु होते हैं।
यह पेंटिंग दो तरह की होती है-भित्ति चित्र और अरिपन या अल्पना। इसमें चटक रंगों का इस्तेमाल खूब किया जाता है। मिथिला लोक चित्रकला की सर्वप्रमुख विशेषता जीवन के हास-विलास,प्राकृतिक संभार एवं अध्यात्म का अंकन है। इसमें जीवन का सम्पूर्ण विस्तार समाहित है और सम्पूर्ण जन-जीवन इसे उत्कीर्ण करने में योगदान देता रहा है। विद्यापति पदावली की भी यही स्थिति है। मिथिला के लोक जीवन के साथ वह एकम एक है।
कविता और चित्रकला में एक अन्तःसम्बन्ध तो बनता ही है। कवि ऐसा चित्रकार होता है,जो बाह्य संसार के बिम्ब को उसी सजीनता से चित्रित करता है,जिस प्रकार चित्रकार वस्त्र वर चित्र अंकित करता है। पश्चिम में कविता और चित्रकला के अन्तःसम्बन्ध पर चिंतन हुआ है,किन्तु भारत में इस संदर्भ में किंचित विस्तृत चर्चा नहीं हुई है। हॉरेस ने अपने आर्सपोइतिका में कविता और चित्रकला के अन्तःसम्बन्ध पर विचार किया है।
यूरोप के पुनर्जागरणकाल और बारोक (अतिशय अलंकारवादी) समीक्षकों ने सौन्दर्यात्मक समीक्षा में एक व्यापक प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए हॉरेस के ”जैसे चित्र में वैसे कविता में’ उक्ति का प्रयोग किया। कवि ऐसा चित्रकार माना गया,जो अपनी योग्यता से बाह्य संसार के बिम्ब को उसी सजीवता से चित्रित करता है,जैसे चित्रकार वस्त्र पर करता है। भारत में कविता और चित्रकला के अंतःसम्बन्ध पर पश्चिम की तरह सिलसिलेवार विमर्श तो नहीं हुआ,पर विद्यापति,सूरदास,बिहारीलाल आदि ऐसे कवि हुए हैं,जिनकी कविता का सादृश्य चित्रकला से रहा है।
कवि नरेन्द्र मोहन ने स्वीकार किया है कि चित्रों के रंग और रेखाओं के साथ संवाद की अवस्था में आने पर उनकी कल्पना के पंख लग जाते हैं। चित्रकला के कुछ ऐसे ही अनुभव-क्षणों में उन्होंने ‘खरगोश के चित्र और नीला घोड़ा’जैसी लम्बी कविता लिखी थी,जिसमें कविता चित्र और सृजन प्रकिया साथ-साथ है। कविता और चित्रकला में माध्यमों की भिन्नता तो है,पर ये अपनी विधागत सीमाओं को तोड़कर एक-दूसरे के करीब आती हैं। चित्रकला की रेखाओं और रंगों की अभिव्यक्तियों कविता की लय में रूपायित होती हैं। विद्यापति पदावली और मिथिला लोक चित्रकला को आमने-सामने रखकर कविता और चित्र की दुनिया में छिपे रचना-सूत्रों की खोज की जा सकती है। सौन्दर्य का सूक्ष्म विश्लेषण,आत्माभिव्यक्तियाँ तथा रहस्यपूर्ण शैली मिथिला लोक चित्र की विशेषता है और यही विशेषता विद्यापति पदावली की भी है। विद्यापति पदावली की प्रत्येक पद अलग-अलग चित्र प्रदर्शित करता है।
विद्यापति सौन्दर्य के कवि हैं। नखशिख वर्णन,सद्यस्नाता-वर्णन,मिलन,अभिसार,वियोग आदि भावों के मनोमय चित्र पदावली में दृष्टिगत होते हैं और उनका रूपांकन मिथिला लोक चित्रकला में दृष्टिगत होता है। श्रीकृष्ण के विरह से व्याकुल राधा कहती है कि वसन्त काल में जब श्रीहरि पुनः वापस लौटेंगे तब वह अरिपन की लिखिया करेगी-”लता तरुअर मंडप दीअनिरमलससधरभित्तिपऊअँ नाल अइपनभल भेल।”
‘रात पल्लव नव पहिरवधबलीयदेल’काव्य और चित्र का माध्यम अलग-अलग है,किन्तु धर्म एक ही है। विद्यापति ने नायक-नायिका के रूप-चित्रण के अंतर्गत अंग-प्रत्यंग की योजना और वेशभूषा का चित्रण किया है,जिसकी सहधर्मिता मिथिला चित्रकला से दिखायी पड़ती है। विद्यापति की राधा कहती है-
”छाड़कान्ह मोर आँचर रे,फाटत नव-सारी।
अपजसहोयत जगत भरि हे,जनिकरिअ उधारी।”
इस प्रसंग में मिथिलांचल में बहुतेरे लोकचित्र दिखायी पड़ते हैं। राधा-कृष्ण की मधुर लीलाओं से पदावली भरी पड़ी है और इनके चित्रांकन से मिथिला लोक चित्रकला। विद्यापतिनखशिख वर्णन के प्रसंग में रेखाओं और रंगों का अद्भुत समायोजन प्रस्तुत करते हैं। सद्यःस्नाता नायिका का यह चित्र तो देखिए
”कामिनिकरेयसनाने,हेरतहिहद्यहनएपँचबाने।
चिकुर गरए जलधारा,जनिभुख-ससि डरें रोअएअँधारा।
कुच-जुएचारूचकेवा,निअ कुल मिलतआनि कोने देवा।
तेसंकाएँ भुज पासे,बाँधिबएलउड़िजाएतअकासे।
तितलबसन तनु लागू,मुनिहुक मानस मनमथजागू।
सुकवि विद्यापति गावे,गुनमतिधनिपुनमत जन पावे।’
विद्यापति पदावली में अपने समय और समाज के यथार्थ और भक्ति से संबंधित पद भी हैं-
जय-जय भैरवि असुर भयाउनि,पशुपति-भामिनि माया।
सहज सुमति बर दिअ हे गोसाउनि,अनुगति गति तुअ पाया।
बासररैनिसबासनसोभित,चरनचन्द्रमनि चूड़ा।
कतओक दैत्य मारिमुँहमेलल,कतेकउगिलिकेल कूड़ा।
सामर वरन नयन अनुरंजित,जलद जोग फुलकोका।
कट-कट विकट ओठ-पुटपाँडरि,लिधुर फेन उठ फोका।
घन-घन-घनन घुंघरू कत बाजए,हन-हन कर तुअ काता।
विद्यापति कवि तुअ पद सेवक,पुत्र बिसरूजनि माता।
इस पद मेंविद्यापति देवी का चित्र खींच देते हैं। कविता और चित्रकला का भेद मिटता प्रतीत होता है। विद्यापति के विविध पदों में चित्रात्मकता स्पष्टतः परिलक्षित होती है। वह मिथिला चित्रकला के प्रभाव से रससिक्त है। उनकी कृति की आधार-भूमि पर मिथिला चित्रकला की परंपरा भी बदस्तर जारी है।
काव्य और चित्र का धर्म एक ही है। सिर्फ दोनों की अभिव्यक्ति का माध्यम अलग-अलग है। रूप-चित्रण से लेकर भक्ति-भाव-वर्णन तक मिथिला चित्रकला का प्रभाव विद्यापति पर दिखायी पड़ता है। वहाँ इस चित्रकला की रेखाओं और रंगों का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। पदावली रेखाचित्रों से भरी पड़ी है। इनका मुख्य आधार,कृष्ण-लीला,नायिका भेद एवं प्रकृति रही है। कृष्ण के रूप-सौन्दर्य के चित्रण में सिरपर मोर-मुकुट गले में वनमाला एवं शरीर पर पीताम्बर चित्रकला की सबल रेखाएँ हैं। पदावली में वर्ण-चेतना भी है। प्राथमिक रंग,सहायक रंग,मध्यवर्ती रंग एवं उदासीन रंग रेखांकित किये जा सकते हैं। विरोधी रंगों के संयोजन से विभिन्न तरह के चमत्कारिक चित्र खींचे गये।
मिथिला लोक चित्रकला की आधार-भूमि लोक जीवन,लोक तत्त्व,लोकोक्ति,अंधविश्वास आदि हैं। यही विद्यापति की काव्य-भूमि है। इसलिए मिथिलांचल में दोनों की लोकप्रियता अप्रतिम है।