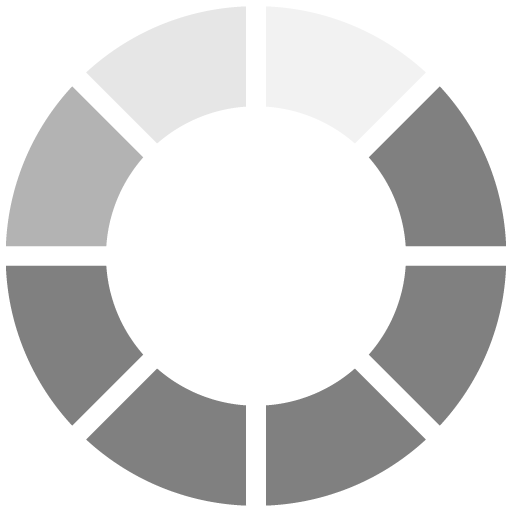मिथक और नदियां दोनों हमारे जीवन से गहरे तौर पर जुड़े है। एक हमारे मानस मे प्रवाहित होती है तो दूसरी धरती पर । किंतु दोनों का ही प्रवाह एक साथ दिक काल में कई तलों व आयामों में होता है। अपनी सीमाओं की वजह से हमारी प्रवृत्ति उसे एकांगी रूप में देखने की होती है नदियों को जलसंसाधन मात्र तो मिथको को फुजूल के खिस्से।
मिथक नाम आते ही आमतौर पर आज लोगों(खासकर युवाओं) के मन में पुरानी पोथियों(खासकर धार्मिक) में कैद एक ऐसी दुनिया की छवि उभरती है। जिसके साथ वर्तमान का कोई संवाद नहीं है कोई सावल नहीं कोई गुफ्तगू नहीं। सो आज की वैज्ञानिक तर्कशील पीढ़ी मिथकों को विज्ञान के मुकाबले कुछ इस तरह से खड़ा करती है कि प्रगतिशील कहाने वाले लोगों को मिथकों में मानव सभ्यता के आगे की यात्रा के हिसाब से सुफेद कम स्याह ज्यादा नजर आता है। वे उसे भूत करार देकर जल्दी से पीछा छुड़ा लेने में ही भलाई समझते है। उनकी माने तो कौतुक व मनोरंजन के लिए आप इसके पास जा सकते हैं पर उसमें रमना जुड़ना वक्त जाया कर फाव में आऊटडेटेड होने का ठप्पा लगवाना है।ये हालात इसलिए है कि छापे के अक्षरों के विकास के बाद से ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया व उसका प्रवाह सामाजिक से कहीं अधिक वैयक्तिक हो चली है।
सामूहिक अवचेतन जो पहले वैयक्तिक व सामाजिक दोनों स्तरों पर हमारी पहचान तय करता था।इसमें सामाजिक स्मृतियों की खासी भूमिका थी। इनमें से कई स्मृतियां दूर क्षीतिज से मिथकों के पास से आती थी। जैसे दूर तारों के पास से आती रोशनी बहुत मद्धम होने की वजह से आम लोगों के लिहाज से किसी काम की नहीं होती पर लैज्ञानिकों के लिए उस रोशनी में ब्रह्मांड के कई राज छिपे होते हैं।
वैसे ही वर्तमान की परिधी में खड़ा आधुनिक मनुष्य अपनी सीमाओं की वजह से कई बार मिथकों में कोई सार कोई अर्थ नहीं खोज नहीं पाता हैं। आज से पहले समाज में ज्ञान श्रुतियों(कथाओ व मिथकों) में प्रवाहमान था। कथाओं की खास भूमिका थी क्योंकि यही समाज के खास व आम अनुभवों को रोचक व पाचक ढंग से समय व समाज में प्रवाहमान करता था। इसी धारा में मूल्य(सामाजिक वैयक्तिक) और उनके जरिये कौशल भी एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक पहुंचते थे, ब्यष्टी और समष्टी दोनों स्तरों पर।
यही कारण है कि अतीत में जनजातीय समाजो में कथावाचकों(स्टोरी टेलर) का महत्व योद्धाओं से कहीं अधिक ही होता था कम नहीं ।मंगोल जिन्होंने एक समय लगभग पूरी दुनिया को जीत लिया था उनके संगठित और सशक्त होने में कथाओं व मिथकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। शिकार उनकी युद्ध शैली का अहम हिस्सा था यही वजह है कि हमारे खिस्से कहानियों में राजा और शिकार अभिन्न रूप से जुड़ गए। मंगोल मिथक कथाओं में एक नायक आकाश में उगे पांच सूरज में चार सूरज को अपने से तीर से नीचे गिरा देता है तो चीनी मिथक कथाओ में नायक यी 10 सूरज में से नौ सूरज से अपने बाणों से नीचे धरती पर गिरा देता है। एक साथ आकाश में पांच चार दस सूरज आज हमारे अनुभव व सोच की परिधी से बाहर है । पर स्कैंडिनेवियाई देशों में आकाश में एक साथ दो या चार सूरज देखने की बात आती है। मिथकों का अर्थ समझने के लिए हमें उसे एक साथ इतिहास, भाषाविज्ञान, भूगर्भशास्त्र के कई बिंदुओं से देखने पऱखने की आवश्यकता है।
मिथक समाज को एक डोर में बांधे रखने और इस तरह उन्हें सशक्त व अर्थवान बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जीवन रस सिक्त और अर्थवान हो उसमें स्मृतियों की महति भूमिका है। स्मृति जहां जिस ठौर अपनी थकान मिटाती है या फिर जहां डुबकियां लागाकर अपने को ताजा दम कर आगे की यात्रा पर निकलती है वो कथाएं ही हैं। कथाओं के घाट पर मन तर्क के तान से मुक्त होता है कल्पना अपने नैसर्गिक प्रवाह में और सृजन अपनी रौ में होता है। कथाओं की उम्र स्मृतियो(वैयक्तिक) से कहीं लंबी होती है। इनकी उम्र कई बार सभ्यताओं से भी बड़ी होती है। यही वजह है कि पुरानी सभ्याताओं के मिथक उसी रूप में या फिर नये रूपों में नयी सभ्यता में आ जाते हैं। कैसे ये कथाएं एक समय की कथा कहते हैं इसका नमूना कहावत से ले सकते हैं एक कहावत है बारीक पटुआ तीत । इसे अगर हम भुला दें तो नयी पीढ़ी को यह पता नहीं होगा की पटसन के पत्तों के साग खाये जाते थे।
कथाओं से भी ज्यादा लंबी होती है मिथकों की। विभिन्न सभ्यताओं के मिथकों को जब हम एक साथ पढ़ते गुनते है तो पाते हैं कि इनमें कई समानताएं है जो एक मूल स्रोत की ओर इशारा करती हैं। मिथकों की दुनियां को जब खंगालते हैं तो पाते हैं कि ये दिक काल में काफी यात्राएं करती है। इस वजह से कई बार धरती के दो कोनों के बीच बसे समाजों के रीति रिवाज एक से होते हैं। कई मिथक कथाओं की संरचना थोड़े बहुत हेर फेर के परे समानधर्मा लगती है।यानी एक ही स्रोत से आती मालूम पड़ती है। ओल्ड टेस्टामेंट की कथा में मिश्र के राजाओं के कोप से बचकर भागते यहुदियों की रक्षा के लिए समुद्र का पानी दो भागों में बंटकर रास्ता दे देता है तो कृष्ण की रक्षा के प्रयत्न में लगे वासुदेव की सहूलियत के लिए यमुना रास्ता दे देती है।
लगातार बढ़ने वाले पर्वत कई देशों की मिथक कथाओं में आते हैं। रावण और शिव की कथा ही ले लीजिए रावण शिव को अपनी अराधना से रिझाकर अपने साथ श्रीलंका ले जा रहा था। देवताओं ने उससे छल कर शिव को वहां वहां जाने से बचा लिया उनके वचन की मर्यादा रखते हुए। वैद्यनाथ धाम की कथा में रावण के साथ जहां विष्णु ने छल किया वही कर्नाटक के गोकर्ण में गणेश ने उसके साथ छल किया। समान प्लॉट वाली एक और कथा तमिलनाडु के त्रिची से मिलती है जिसमें रंगनाथ(विष्णु) को विभीषण द्वारा श्रीलंका ले जाने से रोकने के लिए गणेश ने उनके साथ छल किया। जो लोग भी तिरूपति गये होंगे उन्हें देखा होगा कि वहां बालाजी के स्थान को बैकुंठ बताया गया है।
उत्तर बिहार में गंडक नदी के उपरी हिस्से मे भी एक बैकुंठ है जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रत्येक वैष्णव को जीवन में एक बार इस बैकुंठ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। गंडक नदी का एक ही एक नाम नारायणी या शालीग्रामी भी है। विष्णु के रूप शालीग्राम इसी नदी में मिलते है। भूगर्भ शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए यह एमोनिटिक फॉसिल है जिसे मिथको में बज्रकीट भी कहा गयी है।समुद्र में रहने वाले इस प्राचीन जीव को इंडेक्स फॉसिल का दर्जा हासिल है । यानी इनका पाया जाना इस बात का इशारा करता है कि वहां कभी समुद्र रहा होगा।
एमोनाइट देखने में उपर से भेड़ के सिंग की तरह होता है जिसे एक ग्रीक देवता अपने सिर पर धारण करते हैं कुछ ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार या मिश्र के देवता आमून के साथ मिलता है जिसे बाद में ग्रीक लोगों ने अपना लिया था। मिथक लोक कथा जीवाश्मों के बीच काफी रिश्ते सुनने को मिलते हैं 100 एडी के पास प्लुटार्क ने एजियन समुद्र के पास सामोआ द्वीप को पनैयमा यानी ब्लड बाथ अथवा ब्लडी बैटल फील्ड कहा था। पुरानी इटालवी नक्शों में इस बात की तस्दीक होती है।
ग्रीक मिथकों के अनुसार यहां पर ग्रीक युद्ध देवता डिओनिसियस के हाथी का अमोजोन्स के साथ भयंकर युद्ध हुआ था जिसकी वजह से धरती लाल हो गयी थी। बाद में यहां से भुगर्भ वैज्ञानिकों ने मैस्टोडोन नाम के हाथी के जीवाश्म को खोज निकाला था। असम के तेजपुर जिले में अग्निगढ़ किला है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बाणासुर का किला था। यहां पर कृष्ण व शिव में भयंकर युद्ध हुआ था जिसकी वजह से धरती लाल हो गयी थी। तेजपुर का अर्थ रक्त होता है इसी से सटे दूसरे जिले का नाम शोणितपुर है जिसका अर्थ भी संस्कृत में रक्त होता है।
कथा कल्पना व अनुभव के सहारे जिस दुनिया को रचती है उसका एक सिरा हमेशा हमारी पकड़ में रहता है या तो हमारे देखे जाने दुनिया में या फिर ऐसी दुनिया में जिसे थोड़े हेऱ् फेर के साथ हम अपना मान सकते हैं। मिथकों की कथा कुछ अलग है। वे एक ऐसी कथा है जिसका विस्तार समय व स्पेस में इतना है कि उसके सामने हमारे अनुभव व हमारा ज्ञान अपने हथियार डाल देते है।यानी की वह दिक् काल(टाइम- स्पेस) में एक अलग स्केल पर होती है इसलिए उस दुनिया के किरदार उसके लक्षण चरित्र बिल्कुल अनजान व अजूबे लगते हैं। वैसे ही जैसे भौतिक विज्ञान में जब हम नैनो स्केल पर जाते हैं तो वहां की दुनिया बिल्कुल अलग होती है ।यहां लोहा पारदर्शी भी हो सकता है और कपड़े अपनी सफाई खुद कर सकते हैं।वैसे भी धरती की उम्र को अगर हम स्केल मान तो मानव की उम्र उसमें नैनो स्केल की तरह ही होगा। जीवाश्मों के सहारे जब हम धरती ती कथा पढ़ते है तो कई अक्षर हमारी पहचान के नहीं होते तो कई पन्ने गायब मिलते है मिलते भी है तो सिलसिलेवार नहीं । उसमें कुछ पाने के लिए हमें
उसमें डूबना होता है उसके प्रवाह में अपने को प्रवाहित करना होता है समय व स्पेस दोनों में दूसरे सिरे से यात्रा करनी होती है। मिथकों के ब्यौरे विस्तार और बारीकी दोनों में ही कई बार हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं हमारी कल्पना को झकझोरते हैं इसलिए वे अक्सर कला की दुनिया में दस्तक देते हैं चित्रकला में खास तौर पर।
मिथकों व नदियों की आपस में नातेदारी है इसलिए चरित्र में उनके बीच काफी समानता देखने में आती है। मिथकों व नदियों को लेकर कई समस्याओं की जड़ में हमारी अपनी सीमाएं। जैसे नदियां दिक काल में एक साथ कई तलो और कई आयामों में प्रवाहमान होती है वैसे ही मिथक भी एक साथ कई स्तरों व आयामों में प्रवाहमान होते हैं। अपने प्रवाह के क्रम में वह गुजरने वाले प्रदेशों से संवाद करती चलती है यह संवाद रूप व कथ्य दोनों ही स्तर होती है। समस्या है कि अपनी सीमाओं की वजह से हम उसके सभी स्वरूप को एक साथ नहीं देख पाते जिसके कारण उसके दो स्वरूप एक दूसरे से नितांत भिन्न हो सकते हैं।
जिसने गंगा को सिर्फ बनारस में देखा हो गोमुख के पास नहीं वह यह मानने को कतई राजी नहीं हो सकता है कि आप फांदकर गंगा को पार सकते हैं।जिसने भूगर्भ शास्त्र नहीं पढ़ा हो उसे कम ही पता होता है कि यमुना गंगा के साथ मिलती है यह हर युग के लिए सत्य नहीं है।बागमति गंगा की सहायक नदी भले हो पर उसकी महत्ता थोड़ी भी कम नहीं है इसके लिए हमें मिथकों का छोर पकड़कर उसके साथ यात्रा पर निकलना होता है। यह यात्रा देश व समय दोनों में होती है। नदियों का संगम तीर्थ माना जाता है यह बात केवल प्रयाग या इलाहाबाद के लिए सच नहीं है । चंद्रा और भागा नदियों का संगम जो साथ मिलकर चेनाब नदी का निर्माण करती है बौद्धों के लिए उतना ही पवित्र है।
कैलाश हमारे लिए जितना पवित्र है बौद्धों के लिए भी उतना ही। दक्षिण भारत में पूजा पाठ के अवसर पर जल को तीर्थ ही कहा जाता है। जब हम भारत से नेपाल की ओर रुख करते हैं तो पाते हैं कि जैसे भारत में हिंदुओं की मुक्ति गंगा के बगैर नहीं होती वैसे ही नेपाल में हिंदू और बौद्ध दोनों की ही बागमति के बगैर नहीं होती। यही बात हमें उत्तर बिहार से चलकर झारखंड पहुंचने पर पता चलती है कि भले दामोदर को हम बंगाल के शोक को तौर पर पहचानते हैं पर संतालों को मुक्ति बगैर दामोदर में अस्थि प्रवाहित किए नहीं होती है।नर्मदा व सोन के अधूरे विवाह की कथा भी एक अलग तल पर जाकर हमें उसके पुरातन प्रवाह मार्ग की कथा बताती है।विष्णु के दस अवताओं में दूसरे अवतार कूर्म हैं।
काकीनाडा में इस अवतार की समपर्त मंदिर की असली मूर्ती के बारे में कई लोगों का कहना है कि यह मूलत: एक फॉसिल है। आंध्रप्रदेश में गांवो में मालेरी फॉर्मेशन में पाये जाने वाले ड़ॉयनासोरों के अवशेष के बारे में भी कई रोचक कहानियां सुनी जाती है कि कुछ फॉसिल को स्थानीय लोग देवी मानकर पूज रहे थे। महाबालेश्वर में भी शिवलिंग और उसकी पूजा पद्धती अलग है। एक नजर देखने में एक लावा प्रवाह से जुड़ा मालूम होता है। एक उदाहरण देने से थोड़ी सहूलियत हो सकती है थोड़ी देर के लिए हम कछुओं की दुनिया में चलते हैं उसे मानव की तरह स्मृति व संवाद सामर्थ्य से लैस मान लें। आपने ओलिव ग्रीन रिडले कछुओं के बारे में सुना होगा।
एक लंबा सफर तयकर उनके लिए सागर तट पर आकर कुछ खास जगहों पर अंडा देना और उन अंडो से बच्चे जैसे ही निकलते हैं वे समुद्र की ओर रुख कर लेते हैं।मुझे इसकी वजह पहले नहीं समझ आती थी। पर बात में पढ़ा की एक समय कछुए बेचारे अत्यं निरीह जीव थे। समुद्र उनके लिए एक खतरनाक जगह थी खासकर उनके नवजातों के लिए । उनकी नवजात बचे रहे और उनका वंश चले इसके लिए उन्होंने सागर के बाहर की दुनिया का रुख किया। पर यह अतीत में काफी पुरानी बात है आज के कछुओं के लिए समुद्र उतनी खतरनाक जगह नहीं है पर यह परंपरा आज भी कायम है।
कुछ मछलियां भी इसी तरह का व्यवहार करती है। पता नहीं कछुए आपस में क्या और कैसे संवाद करते हैं उनके स्मृतियों की कितनी आयु होती है। पर थोड़ी देर के लिए उन्हें अपनी तरह मान लें तो कछुओं के लिए भी उनके पहले पूवर्ज की कहानी जिसने अपने बच्चों मिथक की तरह हो जाएगी।
अभी हाल में ही रूस के साइबेरिया में एक गुफा से इस बात के प्रमाण मिले है कि मानव के दो पूवर्ज प्रजातियों निएंडरथल व डेनिस्टोव के बीच यौन संबंध बने थे। मिथक कथाओं के बारे में पढ़ते हुए दक्षिण पूर्व एशिया पूर्वी इंडोनेशिया के केदांग प्रांत में एक कथा ऐसी मिलती है जिसमें एक नायक एक ऐसी नायिका से मिलता है जो देखने में मानव से काफी भिन्न लगती है। बाद में गौर करने पर उसे पता चलता है कि वह कोई राक्षसी या जानवर न होकर एक महिला है और वह उसके साथ विवाह कर लेता है।
हम आज जिस समय-समाज में जी रहे हैं उसमें सूचनाओं का प्रवाह प्रबल है। जिस तेजी से सूचनाओं का प्रवाह हमारी ओर आ रहा है वो हमारे पैरों को हकीकत (समझ) की जमीन से उखाड़ दे रहा है। हमें ठहरकर सोचने की मोहलत ही नहीं देता है। जिंदगी में हकीकत को आभासी दुनिया ने घेर रही है बड़ी होशियारी से होशियार लोग हमारी सीमाओं का इस्तेमाल कर हमें एक ऐसे कोने में धकेल देते हैं जिसमें हम मान बैठते है हमारे अंदर ज्ञान व सत्य को समझने की असीमित क्षमता है इसकी परिधी से जो भी बाहर है वह मायावी है जो मायावी है वो गैर जरूरी है।