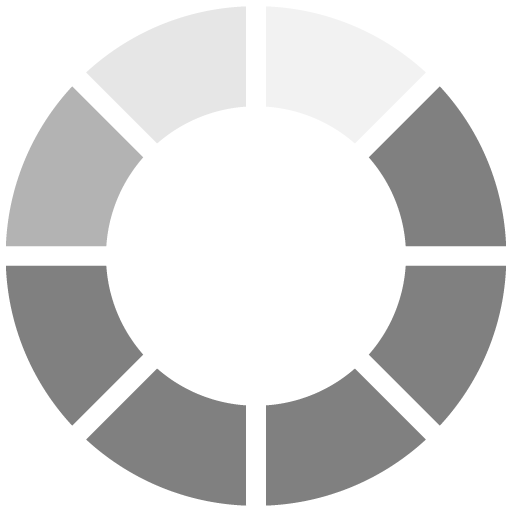संस्कृतियों के उद्भव तथा विकास का स्थानीय पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का अटूट सम्बन्ध है. प्राकृतिक संसाधन पर्यावरण के अनुरूप बदलते रहते हैं तो संस्कृतियाँ भी उसी के संग बदलती हैं और विकसित होती हैं. जहां जंगल ज्यादा हैं वहाँ जंगल आधारित जीवन शैली या संस्कृति का विकास होता है, शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों जीवन पद्धति, रहन-सहन, रीति-रिवाज, खेती-बारी आदि तथा अन्य जीवधारियों से मनुष्यों के सम्बन्ध उसी तरीके से विकसित हुए होंगें. यही बात हिम-आधिक्य क्षेत्र में एक हिम संस्कृति का विकास हुआ होगा.
मिथिला जल-बाहुल्य क्षेत्र था और अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है तो यहाँ जीवनचक्र जल के इर्द-गिर्द घूमता रहा है और अभी भी पानी ही यहाँ की जीवन चर्या को निर्धारित करता है. रेगिस्तान वाले इलाके में अगर हम जाएँ तो वहाँ का सारा परिवेश जल संचय पर आधारित है. सुबह से उठ कर रात तक पानी के स्रोत खोजना, उसे लाना, उसकी सुरक्षा के उपाय ढूँढना और उसे संपत्ति की तरह सहेजना दिनचर्या का अंग होता है. उन क्षेत्रों में आपको दूध यथेष्ट मात्र में पीने को मिल जाएगा पर बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पानी का उधारा चलता है. आज अगर मैंने आप को एक घड़ा पानी दिया तो मैं यह आशा करूंगा कि मेरी जरूरत के समय आप एक घड़ा पानी लौटा देंगें.
उस दृष्टि से मिथिला बहुत ही जल-संपन्न क्षेत्र है कि हमारी महिलाओं के सर पर अभी तक घड़े नहीं दिखाई पड़ते जबकि पश्चिमी राजस्थान में घड़ा महिला की पोशाक का हिस्सा बन जाता है. वहाँ अगर कभी किसी ऐसी महिला को ग्रामीण क्षेत्र में आते-जाते देखें जिसके सर पर घड़ा न हो तो यह उतना ही अजीब लगता है जितना मिथिला क्षेत्र की किसी महिला सर पर घड़ा लगता है.
वहाँ परिवार के एक कम से कम या दो पुरुषों का तो काम बनता है कि ऊँट गाड़ी लेकर निकल जाएं और पानी की व्यवस्था करें. उन लोगों ने पानी को संचित रखने और उसे सुरक्षित रखने में ग़ज़ब का कमाल हासिल किया है. जहां तक मिथिला में पानी की स्थिति है, वहाँ आज भी ‘मुस्कुराइए कि आप मिथिला में हैं.’ हमें यहाँ मित्रों से शर्त नहीं लगानी पड़ती कि बारिश होगी तो ओरीचूएगी या नहीं, नाली बहेगी या नहीं आदि आदि. यह सब कम पानी वाले क्षेत्रों की समस्याएं हैं यहाँ बरसात होगी तो झमाझम होगी और वह किसी शर्त के दायरे में नहीं आती.
हमने पानी के प्राचुर्य के साथ जीना सीखा. उसी के हिसाब से हमने अपने घरों की डिजाइन तैयार की, स्थानीय गृह-निर्माण सामग्री से अपने घर बनाए, उसी के अनुरूप अपने कृषि-चक्र को तैयार किया, उसी पर आधारित अपनी फसलों और बीजों का चयन किया और उसी को ध्यान में रख कर पानी के मूल स्रोत नदियों के साथ रिश्ते स्थापित किये. उनका माता, से लेकर भूतनी, वक्रा (बकरा), डाइन आदि तक का नामकरण किया. हमारी कोसी एक ऐसी नदी है जिसे माता और डाइन दोनों का दर्ज़ा समान रूप से हासिल है.
यह निर्भर इस बात पर करता है कि नदी आज हमारे साथ कैसा सलूक कर रही है. हमने उन्हें कन्याओं की तरह स्वछन्द रूप में देख कर उछलते कूदते देखा है जैसा मिथिला की अधिकाँश नदियाँ हैं. वह एक जगह स्थिर नहीं रहतीं. कोसी, बागमती, कमला, महानंदा और अधवारा समूह की अनेको नदियाँ इसके उदाहरण हैं.
वहीँ नारायणी (गंडक) और गंगा विवाहिता इसलिए हैं वो कन्याओं की तरह उछल कूद नहीं करतीं. पर्वत से आने वाली तमाम नदियों को हमने पार्वती कह कर उनका मान बढाया है तो हमारी सिकरहना एक पातालफोड़ नदी है. इन सारी नदियों के साथ पौराणिक और लोक-कथाएँ जुड़ी हैं. पुराण तो लिपिबद्ध हैं मगर लोक कथाओं का हमारे यहाँ टोटा जरूर है.
इन नदियों और सरोवरों से समृद्ध मिथिला ने सिंचाई की व्यवस्था विकसित की थी. उपजाऊ ज़मीन और बारहों महीने उपलब्ध जल ने अकाल या दुर्भिक्ष से मिथिला को साधारणतः दूर रखा. अगर कभी ऐसी परिस्थिति आई भी तो वह जल, जंगल और ज़मीन के कुप्रबंधन और शासकों के लोभ के कारण आयी, समृद्ध पर्यावरण पर पड़े दबाव के कारण नहीं. अट्ठारहवीं शताब्दी के मध्य में अँगरेज़ भारत में सत्ता में आये. अगले लगभग सौ वर्षों में उन्होनें यहाँ की सिंचाई और कृषि के क्षेत्र में बहुत से प्रयोग किये पर उनका उद्देश्य आम जनता की भलाई का उतना नहीं था जितना अपने ज़खीरे भरना.
उन्होनें देश के सूखे वाले क्षेत्र में सफलता भी अच्छी पायी और तब उनकी नज़र इस जल-संपन्न क्षेत्र पर भी पड़ी. उनको लगा कि अगर इस क्षेत्र को बाढ़ से मुक्त कर दिया जाय तो बाढ़ मुक्ति के नाम पर उनकी कमाई हो जायेगी और जब बाढ़ नहीं रहेगी तो सिंचाई की जरूरत पड़ेगी और तब वह उसमें भी कमाई कर लेंगें. उन्हें लगता था कि ऐसा करके वो सूखे वाले क्षेत्रों से ज्यादा पैसा बाढ़ वाले इलाके से बना लेंगें.
उन्होनें बंगाल और उड़ीसा में काफी कोशिशें भी कीं और मुंहकी खाई. जल-संपन्न नदियों ने तो उन्हें अपनी पूरी नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया था. 1870 के आसपास उन्होनें कसम खाई की वो जब तक भारत में रहेंगें, हिमालय से आने वाली और भारी मात्रा में गाद लाने वाली नदियों को कभी बाढ़ नियंत्रण के लिए हाथ नहीं लगायेंगे. यह कौल उन्होनें1947 तक रखा जब तक वो यहाँ से हमेशा के लिए चले नहीं गए.
उनके जाने के बाद आज़ाद भारत में हमने अपने पारम्परिक नजरिये की ओर ध्यान न देकर उन तकनीकों को आगे बढ़ाया जिसमें न तो स्थानीय परिवेश, फसल चक्र, सिंचन व्यवस्था, निर्माण सामग्री और स्थानीय बीजों का ध्यान रखा और न ही अंग्रेजों की गलतियों से कोई सीख ली. जहां अँगरेज़ उत्तर बिहार के सन्दर्भ में अपनी सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की तकनीक को अव्यावहारिक बता कर हाथ खींच चुके थे उसी को आधुनिकता के नाम पर हमने स्वीकार किया और उसे ही विकसित किया.
शायद यहीं हमसे गलती हो गई. रोटी, कपडा और मकान किसी भी मनुष्य की बुनियादी जरूरतें हैं जिसकी व्यवस्था स्थानीय परिवेश, संसाधन और परंपरा से कर लेनी चाहिए थी जिसमें आधुनिक विज्ञान हमारी मदद करता. रोटी, कपडा और मकान के इन तीनों क्षेत्रों में हमने एक ऐसी बुनियाद पर भवन खड़ा करने का प्रयास किया जो टिकाऊ हो ही नहीं सकता था और वही हुआ. आज हम अगर पलायन न करें तो हमारे घरों में चूल्हे न जलें.
इस विषय पर हमें चिंता और चिंतन जरूर करना चाहिए. हमें अपनी समस्या का समाधान अपने संसाधनों परिवेश, पारंपरिक ज्ञान और जनोन्मुख विज्ञान के सामंजस्य में ही खोजना चाहिए. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इश्वर की श्रेष्ठ कृति ही प्रकृति है और जब हम प्रकृति से कोई छेड़-छाड़ करते हैं तो एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि हम किसके मुकाबले खड़े हैं.