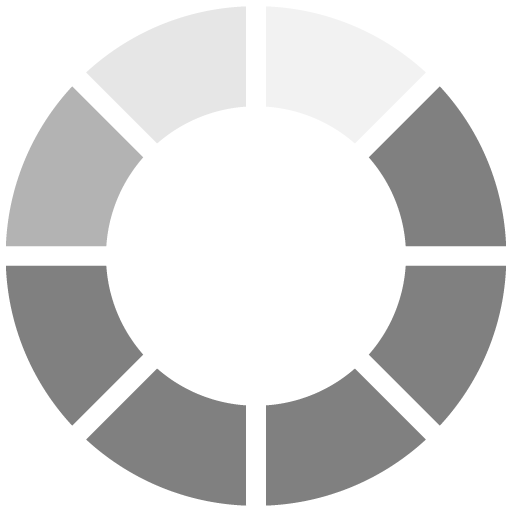बचपन में दरभंगा से बाबाधाम जाने के रास्ते में सिमरिया पड़ता था। वहां गंगा स्नान करने और एक रात बिताने के बाद गंगा के उस पार हथिदह से ट्रेन पकड़ हम देवघर पहुंचा करते। वापसी भी सीधे नहीं हुआ करती। मोकामा, बरौनी या समस्तीपुर में ट्रेन बदलना होता। भीड़ से लबालब भरे ट्रेन। ऊपर से भीषण गर्मी। हम बच्चों को खिड़की के माध्यम से घुसा दिया जाता। वापसी में आते वक्त जसीडीह स्टेशन के बाहर से सुड़ाही खरीद पानी भर लिया जाता। लेकिन गर्मी, भीड़ और ट्रेन के देर होते जाने की नियति का मिला जुला असर भुख और प्यास में निकलता। सिग्नल पर गाड़ी घंटों खड़ी हो जाया करती और खीरा, ककड़ी या ‘फिर लिट्टी खाओ पानी पियो’! यही हमारे लिये बरदान की तरह आते। मांग इतनी हुआ करती कि इन शब्दों को सिग्नल पर सुन लेना और इनके मिल जाने की हकीकत के बीच निराशा से मन और आंखें कई कई बार खाली ही लौट आती।
खैर, बचपन बीता और वह समय भी बीत गया। पिछले कई दशकों से भुख और प्यास को जैसे भुल ही बैठा था। पिछले दिनो, लौट रहे प्रवासी मजदूरों के चित्रों में, वायरल वीडियो ने भुला दी गयी भुख और प्यास को फिर से सामने खड़ा कर दिया है।
सबसे पहले ट्रेन की पटरियों पर कटकर मर गये मजदूरों की पोटलियों से निकल कर रेल की स्टील पटरियों की पहरेदारी में रोटियां दिखाई दी। फिर, कटिहार जंक्सन पर खाने के पैकेट के लिए झगड़ते प्रवासी मजदूरों का वायरल वीडियो। फिर तो जैसे सैलाव ही आ गया हो। उससे पहले भी खाने को लेकर होती झड़पों की खबरें आने लगी थी। दिल्ली में प्रवासी मजदूरों के शैल्टर हॉम के आग लगने की खबर, यमुनाकिनारे निगम बोध घाट के शमशान के निकट मॄत शरीर के साथ मॄत आत्मा के लिये छोड़ दी गयी केले को चुनते प्रवासियों की तस्वीरें और राशन की लंबी कतारों में इंतजार करती पथराई आंखें।

फोटो : गूगल
अभी कल परसों इटारसी स्टेशन पर खाने के पैकेट को लेकर मचे भगदड़ का दॄश्य। सभी कुछ सामने ही तो है।
रेणु के कथा रिपोर्ताज, ‘हड्डिया का पुल’ से टहलु मुसहर की पुतोहु भगिया का चेहरा निकल कर सामने आ जाता है। “पुल से दो मील उत्तर एक ‘चौर’ में ‘करमी’ और सारुख’ खोजनेवाले भूखों की जमात ने आंखों पर उँगलियों का ‘शेड’ डालकर देखा…
‘ठीक वैसा ही! विशाल! लाल! काली माई की जीभ की तरह लाल…।’ “
नहीं! ऐसा कतई नहीं है कि भूख और प्यास हमारे बीच से गायब हो गया हो। यह हमेशा से साथ रहा। बस्तर और कालाहांडी की तस्वीरों और रपटों में हम मिलते रहे। फिर, कभी न थमने बाला किसानों की आत्महत्या। लेकिन, यहां भूख से अघिक कर्ज के बोझ से दमित किसान और उनकी लाचारी ही दिखती रही कुछ कुछ मदर इंडिया सिनेमा से निकलकर आती तस्वीरों की तरह।
पर इन सभी तस्वीरों में भुख आपदा और गरीबी के साथ जुड़कर आती रही।
पहली दफा, प्रवासी मजदूरों के साथ भूख ने इस कदर तालमेल बैठाया हो, ऐसा लगता है इन वायरल वीडियो से। इससे पहले भूख भूमिहीन कॄषि मजदूरों को माईग्रेंट के लेबल के साथ शहरों में ला पटकता रहा। लेकिन एक दफा प्रवासी बन जाने के बाद भूख जैसे उन तस्वीरों से गायब ही हो जाता था। हम श्रम की महत्ता की बात करने लग जाते।
तस्वीर आपको कई दिशाओं में ले जाते हैं, कुछ कुछ कविताओं की तरह
और मुझे याद आता है चट्टोप्रसाद भट्टाचार्य द्वारा 1943-44 के बंगाल के अकाल को चित्रित करते स्केच। सत्यजीत रॉय और ख्वाजा अहमद अब्बास के सिनेमा। बूट पॉलिस…और जागते रहो का प्यास।
नहीं! यह हिंदुस्तान को देखने के उस साम्राज्यवादी एवं प्राच्यवादी नजरिये से बिल्कुल उलट था जिसमें हिंदुस्तान को गरीबी पिछड़ेपन और भूख से त्रस्त ही दिखाया जाता या जहां महज राजा या रंक ही मिलते। जब उन्नीस सौ तीस के दशक में अमॄता शेर गिल आदिवासी औरतों का चित्र बना रही थी तो वहां इनके चेहरों पर गरीबी, सादगी, सहमी ठहरी सी भावनाओं के साथ एक अजीब सा स्वाभिमान भी मिलता है जिससे पूरे कैनवास में एक अदभुत ग्रेस आ जाता है। 1936 में यूं ही तो उन्होनें मदर इंडिया के पेंटिंग हेतु आदिवासी चेहरा नहीं चुना।
वे बीते दशक के कैथलीन मेयो की मशहूर छवि मदर इंडिया को बड़े प्रभावशाली तरीके से सवभर्ट कर रही थी। भारत की एक नयी छवि गढ़ रही थी। सत्यजीत रॉय, चट्टो प्रसाद भट्टाचार्य, ख्वाजा अब्बास, प्रेमचंद, ताराशंकर बंदोपाध्याय, रेणु या अमॄता शेर गिल जिस भुख और गरीबी और पिछड़ेपन को सामने ला रहे थे वह न तो प्रकृति प्रदत्त था न ही सभ्यता जनित। वह मानव निर्मित था। हमारे बीच से, हमारे द्वारा निर्मित। इसीलिये तो निराला का भिक्षुक कहीं ऊपर से नहीं टपकता है। वह चलकर आता है ऐर अचानक से सामने आ जाता है।
“वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता
पेट पीठ दोनो मिलकर हैं एक चल रहा लकुटिया टेक,
मुट्ठी भर दाने को – भूख मिटाने को…”
मन भटकता है। कभी बंगाल का अकाल तो कभी उन्नीसवीं सदी के अंत के मिथिला की ओर जहां अकाल का छंद कवित्त अकाली रचा जा रहा है। दुर्भिक्ष! माइक डेविस की किताब याद आती है। अकाल माने हॉलोकॉस्ट। वहां तो जनसंहार साम्राज्यवादी है।
विभाजन के दौरान भी तकरीबन पंद्रह मिलियन लोग घर से बेघर हुए। विभाजन की हिंसा के लिये भी हॉलोकॉस्ट/जनसंहार की उपमा का प्रयोग कुछ लोग करते हैं लेकिन, वहां भी कुछेक उद्दरणों के (जैसे पाकिस्तान के कब्जे बाले कश्मीर यथा मीरपूर आदि) अलाबे सामुहिक हिंसा या विस्थापन के दर्द में भूख की छवियां मानो छुप सी गयी कहीं। एक कारण पंजाब और बंगाल दोनो ही जगहों की खास भौगोलिकता रही हो। फिर, यात्रा कितनी ही दुरदांत और लंबी क्यों न हो, वह गुजरात और बंबई से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उडीसा की, हजार दो हजार किलो मीटर की नहीं थी।
और, हम रह जाते हैं इन भूख की तस्वीरों के साथ। निपट अकेले। असहाय। इतिहास ने अबकी बार इस भूख के साथ घर छोड़ते हुए नहीं बल्कि घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के चेहरों को जोड़ दिया हो जैसे।